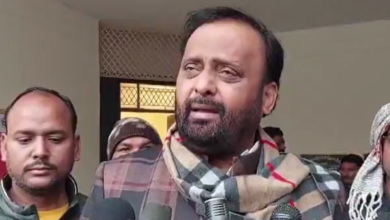दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन कैसे बनी? कितनी है कीमत? जानें सबकुछ

नई दिल्ली. एक ऐसी वैक्सीन (Corona Vaccine) जिसकी कीमत पानी की बोतल से भी कम हो, एक वैक्सीन जिसमें जितना खर्च आएगा, उससे ज्यादा महंगा तो पिज्जा लोग खा लेते हैं. ये वही वैक्सीन है जो तब खबरों में आई जब भारत ने 1500 करोड़ रुपए एडवांस देकर इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज़ का ऑर्डर दिया.
50 रुपए कीमत में एक डोज मिलने वाली इस वैक्सीन का नाम है ‘कोर्बेवैक्स’. इसकी कीमत जितनी तय की गई है उतने में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है. हालांकि बाज़ार में ये 250 रुपए में उपलब्ध होगी. तब भी ये दूसरी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है. वैक्सीन को बनाने वाले का कहना है कि किसी भी चीज़ की कीमत इस बात पर तय होती है कि आप मुनाफा कमाना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं. पिछले साल जब mRna और वायरल वैक्टर वैक्सीन दुनिया में हलचल मचाए हुईं थी, उस दौरान वे चुपचाप एक असरदार इलाज पर ध्यान लगाए हुए थे.
ये कोरोना के खिलाफ युद्ध है
कोर्बेवैक्स का निर्माण भले ही हैदराबाद की बायोलॉजिकल–ई में किया जाएगा लेकिन इस वैक्सीन को विकसित टेक्सास में बेयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में बच्चों के अस्पताल के वैक्सीन विभाग ने किया था. वैक्सीन को विकसित करने वाले सेंटर के को-डायरेक्टर पीटर होटेज ने वैक्सीन विकास पर 20 साल दिए हैं. 2011 में इन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सार्स जैसी बीमारियों के लिए कम दाम वाली वैक्सीन का निर्माण करना था.
उनके नेतृत्व में वैक्सीन पर काम हुआ जिसका नाम CoVRBD219-N1 था, पर इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ. लेकिन जब पिछले साल कोविड ने अपने फन फैलाना शुरू किए तो इस वैक्सीन पर फिर से विचार शुरू हुआ क्योंकि सार्स और कोविड वायरस एक दूसरे से संबंध रखते हैं. जिस तरीके और विधि से वैक्सीन तैयार की जा रही थी, उसी तरीके को इस्तेमाल करके कोविड-19 पर काम शुरू हुआ था. इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करके कैसे वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके. इसके दाम पर भी असर ना पड़े.
असली काम, कम दाम
जिस दौरान कम दाम वाली वैक्सीन का विकास किया जा रहा था. उसी दौरान सेंटर आर्थिक अभाव से जूझ रहा था. हस्टन क्रोनिकल में छपी एक खबर के मुताबिक बेयलर कॉलेज को अमेरिकी सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली थी. महामारी के दौरान शुरुआती महीनों में होटेज का ज्यादा ध्यान वैक्सीन विकास के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ था.
जब लैब की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी तब उन्हें ऐसी जगह से मदद मिली जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाली. टेक्सास स्थित डिस्टिलर टीटोज वोदका ने मई 2020 में लैब को 10 लाख डॉलर की मदद देने की पेशकश की.
सबके लिए, निर्माण भी, कल्याण भी
वैक्सीन की कीमत को कम रखने के लिए सेंटर ने इस पर किसी तरह का कोई पेटेंट नहीं रखा. बल्कि इसके फार्मूले को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, यानि कोई भी इस तरीके का इस्तेमाल करके वैक्सीन निर्माण कर सकता है. इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि इस तरह से अविकसित और विकासशील देशों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहे. होटेज का कहना है कि वैक्सीन को पेटेंट नहीं करवाने के पीछे एक वजह और भी है. किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन पेटेंट करवाने की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है. हमें बमुश्किल काम करने के लिए आर्थिक मदद मिली थी. अगर हमारे पास एक लाख डॉलर हैं तो हम उसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों को सैलरी देने में करेंगे ना की पेटेंट की फीस चुकाएंगे.
जनता की वैक्सीन, जनता के लिए
मार्च में होटेज ने कहा कि ये वैक्सीन पैसा कमाने के लिए नहीं जनता के लिए है. इसका इस्तेमाल गरीब और कम आय वाले देशों में किया जा सकता है. होटेज महीनों तक ये बात कहते रहे कि ये वैक्सीन दुनिया की सबसे कम दाम (110 रुपये) वाली वैक्सीन है. उसके पीछे ये वजह है कि इसे बनाने में वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया गया, जिससे 1986 में हेपेटाइटिस –बी वैक्सीन को बनाया गया था.
इस वैक्सीन को ‘यीस्ट में माइक्रोबियल फरमेन्टेशन’ से तैयार किया जाता है. हालांकि ये बेकरी में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट नहीं है, वैसे तो उसके इस्तेमाल से भी कुछ वैक्सीन बनाई जाती हैं. लेकिन इस वैक्सीन के लिए ‘पिचिया पास्तोरिस’ नाम के यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ये यीस्ट एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसकी मदद से वायरस बड़ी मात्रा में खुद को इंसानों की कोशिका से चिपक लेता है. इस तरह वैक्सीन विशुद्ध प्रोटीन के उपयोग से तैयार की जाती है.
होटेज का कहना है कि ये वैक्सीन साधारण और बगैर किसी लाग लपेट के तैयार हो जाती है. खास बात ये है कि जितना आसान इस वैक्सीन को बनाना है उतना ही इसका संग्रहण भी है. इसे किसी भी साधारण रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है. अब तक इस तरह कि दूसरी वैक्सीन जिसे ‘रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन’ कहते हैं, कई सालों के प्रयोग से ये साबित हो चुका है कि ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित होती है.
क्या अलग है कोर्बेवैक्स में
टेक्सास में बच्चों के अस्पताल में विकसित वैक्सीन को हैदराबाद के बायोलॉजिकल-ई में बनाया जा रहा है. इस वैक्सीन को ‘रिकॉम्बीनेंट प्रोटीन सबयूनिट’ या रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) वैक्सीन के नाम से जाना जाता है. इस वैक्सीन के 28 दिनों के अंदर दो डोज इंट्रामस्क्यूलर दिए जाते हैं. इसे साधाराण रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जा सकता है.
दरअसल 1980 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि किस तरह से दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए को जोड़ा जा सकता है. इसे रिकॉम्बीनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा गया. जब वायरस के जेनेटिक कोड को यीस्ट सेल में डाला जाता है, तो यीस्ट सेल वायरस प्रोटीन बनाने लग जाता है. वैक्सीन निर्माता इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन का निर्माण करते हैं.
आरबीडी वैक्सीन- कोरोना वायरस अपने शरीर के ऊपर लगे स्पाइक (कोरोना के आभासी चित्र में जो कांटे सी संरचना है वो स्पाइक कहलाती है) का इस्तेमाल करके इंसानों की कोशिका से चिपक जाता है. स्पाइक के भीतर, एक हिस्सा होता है जो ‘रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन’ या आरबीडी कहलाता है. वो इंसान की कोशिका में ठहर कर उसे संक्रमित कर देता है. आरबीडी सबयूनिट वैक्सीन जैसे कोर्बेवैक्स में वायरस के इसी आरबीडी प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है.
वैक्सीन के प्रकार
असली वायरस से– इस वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले वायरस को कमज़ोर करके या मारकर वैक्सीन तैयार की जाती है. जैसे कोवैक्सीन
वायरल वैक्टर– इस तरह की वैक्सीन में किसी दूसरे वायरस में बीमारी पैदा करने वाले वायरस का जेनेटिक कोड डाला जाता है, जो वायरस के विशेष हिस्से जो बीमार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है उसका निर्माण करता है. जैसे कोविशील्ड
प्रोटीन सबयूनिट– इसमें वायरस का वो हिस्सा मौजूद रहता है जो बीमारी पैदा करने की वजह है, जिससे इम्यून सिस्टम उसकी पहचान कर सके. जैसे कोर्बावेक्स
एम आरएनए– इस तरह की वैक्सीन में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे वायरस के उस हिस्से को बनाने के लिए निर्देश मिले होते है जो बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है. जैसे फाइजर वैक्सीन.